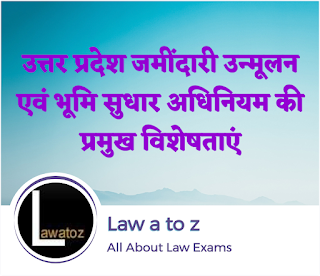उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
State the salient features of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1951, discussing briefly each of them.
इस अधिनियम के नाम से ही परिलक्षित होता है कि यह अधिनियम दो भागों में विभक्त है-
(1) जमींदारी उन्मूलन,
(2) भूमि सुधार।
प्रथम भाग को 1 से 6 तक के अध्यायों में वर्णित किया गया है व दूसरे भाग में 7 से 13 तक सम्मिलित है। अधिनियम राज्य की प्राचीन भू-धृति को एक नया रूप प्रदान करता है।
इस अधिनियम की विशेषताएँ निम्नलिखित है -
अधिनियम की विशेषताएं (toc)
जमींदारी प्रथा की समाप्ति
जमींदारी प्रथा की समाप्ति इस अधिनियम की प्रमुख अन्तर्निहित विशेषता है। निहित होने के दिनांक (1 जुलाई, 1952 ई.) से राज्य सरकार में जमींदारों के सब अधिकार, आगम एवं हित निहित हो गए। जमींदारों के अधिकार न केवल भूमि में बल्कि भूमि के निचले भाग (subsoil) में एवं अकृषित भूमि बंजर आदि में भी समाप्त हो गए।
प्रतिकर का भुगतान
प्रतिकरका भुगतान करना इस अधिनियम की द्वितीय प्रमुख विशेषता है। जिन मध्यवर्तियों के अधिकारों, हकों एवं हितों का अर्जन किया गया, उन्हें उस परिसम्पत्ति (assets) अर्थात् शुद्ध वार्षिक आय के अ आठ गुने के बराबर प्रतिकर (मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) में दिखाई गई है। यह प्रतिकर अधिकारों के निहित होने की तिथि से देय होगा।
पुनर्वास-अनुदान का भुगतान
इस अधिनियम के अन्तर्गत, प्रतिकर के अतिरिक्त मध्यवर्तियों को पुनर्वास-अनुदान भी प्रदान करने की योजना है। इस अनुदान के हकदार जमीदारों के ठेकेदार नहीं है। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इसका निर्धारण प्रत्येक मामलों में अलग-अलग किया जायगा। यह पुनर्वास अनुदान अधिनियम की अनुसूची के अनुसार अनुक्रमिक दर (graded scale) पर 20 गुने से लेकर, देय भू-राजस्व की राशि के बराबर तक का होगा। यदि किसी मध्यवर्ती के द्वारा देय सालाना मालगुजारी दस हजार रुपए से बढ़ जाती है तो उसे कोई भी पुनर्वास अनुदान नहीं प्रदान किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो जमींदार दस हजार रुपए सालाना तक या उससे कम के मालगुजारी हैं उन्हें प्रतिकर भी मिलेगा और पुनर्वास अनुदान भी।
जोत के अधिकारों की सुरक्षा
इस अधिनियम के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, चाहे वे जमींदार हों अथवा काश्तकार अथवा शिकमी काश्तकार, अपनी जोत की भूमि पर कब्जे एवं कृषि करने का अधिकार होगा। परन्तु जमींदार के कब्जे में जो भूमि थी तो वह उसे काश्तकार की हैसियत से रखेगा। भूमि विधि की यह नीति रही है कि जो व्यक्ति भूमि में खेती करता है, वह उसे धारण करे। परिणामस्वरूप हर जमींदार अपनी खुदकाश्त एवं न उठाई गई सीर-भूमि का भूमिधर हो गया। इसी प्रकार प्रत्येक शिकमी काश्तकार अपने कब्जे की भूमि का अधिवासी हो गया।
नवीन भू-धृति व्यवस्था
अधिनियम ने प्राचीन भू-धृति व्यवस्था को समाप्त करके एक नवीन भू-धृति व्यवस्था का सम्पादन किया है। अधिनियम के पहले 14 किस्म की क्लिष्ट एवं भ्रामक जोतदारी व्यवस्था थी। अधिनियम ने जमींदारी प्रथा के साथ-साथ इन जोतदारियों को भी समाप्त कर दिया और समाप्त करके इन्हें चार जोतदारियों में रखा -भूमिधर, सीरदार, अधिवासी एवं आसामी ।
भूमिधर को स्थाई, वंशानुगत तथा अन्तरणीय अधिकार प्रदान किए गए। सीरदार को स्थाई व वंशानुगत तथा आसामी को केवल वंशानुगत अधिकार दिए गए।
अधिवासी की स्थिति सीरदार से कुछ तुच्छ तथा आसामी से श्रेष्ठ थी। यह जोतदारी का एक अन्तरिम स्वरूप था, जिसे पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाना था।
बाद में उ. प्र. भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1954 द्वारा 30 अक्टूबर, 1954 से समस्त अधिवासियों को सीरदार बना दिया गया।
इस प्रकार भूमि के तीन प्रकार के स्वामी, भूमिधर, सीरदार व आसामी रह गए। सीरदार को यह अधिकार था कि वह अपने वार्षिक भू-राजस्व का दस गुना (बाद में 20 गुना) धन जमा करके वह भूमिधर बन जाता था तथा भूमिधरी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता था।
उ. प्र. भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा 28 जनवरी, 1977 से सीरदार की श्रेणी के जोतदारों को समाप्त कर दिया गया तथा भूमिधर को दो श्रेणियों संक्रमणीय भूमिधर व असंक्रमणीय भूमिधर में विभाजित कर दिया गया। समस्त सीरदार संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में माने गए व ऐसे सीरदार जिन्हें ग्रामसभा की भूमि पर सीरदार के रूप में प्रवेश दिया गया, असंक्रमणीय भूमिधर माने गए।
भूमि को लगान पर उठाने का प्रतिबन्ध
अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जब तक वह धारा 157(1) में वर्णित अक्षम व्यक्ति न हो अपनी भूमि को लगान पर नहीं उठा सकता, यदि वह ऐसा करता है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को भूमि उठाने का अधिकार दिया गया है, वे शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हैं, या उन्हें कानूनी क्षमता प्राप्त नहीं है, या इस परिस्थिति में हैं कि स्वयं कृषि नहीं कर सकते, जैसे-अवयस्क, जड़, पागल, अन्धा व्यक्ति, जेल या निरोध में पड़ा हुआ व्यक्ति, आदि।
अलाभकर जोत के निर्माण पर रोक
यह अधिनियम घाटे की जोतों के जमाव को बचाने के लिए जोतों के भावी विभाजन की मनाही करता है। अतः इस अधिनियम के अनुसार 3 एकड़ (पाँच बीघा) से कम की जोत के बँटवारे की आज्ञा नहीं है। यदि बँटवारे की भूमि 3 एकड़ या उससे कम है तो न्यायालय इस भूमि के विकय की अनुमति देगा और प्राप्त आय का बँटवारा हक के अनुसार किया जाएगा।
अधिक भूमि के जमाव पर रोक
भविष्य में कोई भी कुटुम्ब दान या विक्रय द्वारा ऐसी जोत न प्राप्त करेगा, जो उसकी अपनी जोत मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 12 एकड़ से अधिक भूमि हो, जिनके पास 12 एकड़ से अधिक भूमि है, वह उनके पास बनी रहेगी, किन्तु ऐसे लोग कोई और भूमि दान या विकय द्वारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
समान उत्तराधिकार
इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व कुछ जोतदार अपनी वैयक्तिक विधि (Personal Law) द्वारा शासित होते थे तथा कुछ उ. प्र. काश्तकारी अधिनियम, 1939 द्वारा। इस अधिनियम द्वारा उत्तराधिकार के लिए सभी वर्ग, धर्म व जातियों के लिए समान नियम बनाए व वैयक्तिक विधि के उत्तराधिकार पर रोक लगा दी गई। किसी भी जोतदार की मृत्यु पर अधिनियम की धारा 171 से 175 तक के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराधिकार के उपबन्ध किए गए। उत्तराधिकार की यह विधि समस्त भूमिधरों व आसामियों पर समान रूप से लागू होती है।
ग्रामीण जनतन्त्र की स्थापना
इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व ग्रामों में गाँव पंचायत व ग्राम सभाएँ कार्यरत थीं। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार ने जमींदारों से अर्जित भूमि को ग्राम सभा में निहित कर दिया व भूमि के प्रबन्ध के लिए एक भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना कर दी गई। ग्राम सभा की ओर से ग्राम की समस्त भूमि को जैसे आबादी-स्थल योग्य भूमि, रास्ते, बंजर, जंगल, मीनाशय, तालाब, पोखर आदि का भूमि प्रबन्धक समिति को पर्यवेक्षण, संरक्षण तथा नियन्त्रण का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अधिनियम ने ग्रामीण जनतन्त्र की स्थापना की।
निजी कुएँ. आबादी के वृक्षों व भवन तथा संलग्न भूमि का स्वामित्व
अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जिस व्यक्ति का निजी कुओं, आबादी के वृक्षों, भवन तथा संलग्न भूमि (Improvement or appertinent land) उसी व्यक्ति के पास रहने दी गई जिनका उन पर स्वामित्व था अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भवनों व उससे संलग्न भूमि आबादी के वृक्षों निजी कुओं के स्वामी हो गए ।